पश्चिम की तरफ देखने की प्रवृत्ति
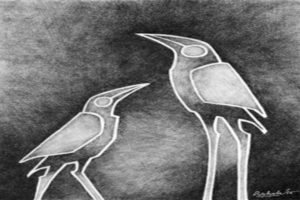
सौ वर्षों की औपनिवेशिक गुलामी का सांस्कृतिक असर सर्वाधिक गहरा पड़ा है। राजनीतिक गुलामी से तो हम सत्तर साल पहले मुक्त हो गए, पर सांस्कृतिक गुलामी की निरंतरता बनी हुई है। आज भी भारतीय बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों में अपने देश के साहित्य, संस्कृति और इतिहास को पश्चिमी नजरिए से देखने की प्रवृत्ति हावी है। हद तो तब हो जाती है जब पश्चिम में लिखे गए साहित्य और उस साहित्य के आधार पर विकसित साहित्य-सिद्धांतों के निकष पर भारतीय साहित्य को कसा जाता है। यह प्रवृत्ति अन्य भारतीय भाषाओं में कम और हिंदी में अधिक है। हिंदी में लिखे जा रहे अधिकतर आलोचनात्मक लेखों में विदेशी साहित्य और विद्वानों के उद्धरणों की भरमार होती है। कई बार तो लेख की शुरुआत ही उद्धरण से होती है। ऐसे उद्धरणों वाले लेखों को हिंदी में काफी प्रतिष्ठा भी मिल जाती है। यह प्रश्न कोई नहीं पूछता कि आखिर भारतीय परिस्थितियों में रचे गए साहित्य का मूल्यांकन, गैर-भारतीय परिस्थितियों में विकसित सिद्धांतों से कैसे हो सकता है? क्या भारतीय साहित्य परंपरा में कोई विचार सिद्धांत या रचना नहीं है, जिसके आधार पर किसी कृति या प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जा सके? ऐसा क्यों होता है कि हिंदी का आलोचक अपनी स्थापनाओं के लिए पश्चिम से वैधता हासिल करता है?
